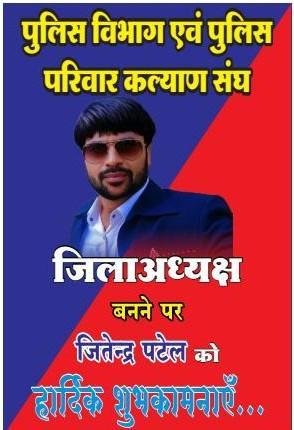लैंगिक समानता की राह में भारत की गिरावट: एक चिंताजनक संकेत : प्रियंका सौरभ

लैंगिक समानता की राह में भारत की गिरावट: एक चिंताजनक संकेत : प्रियंका सौरभ
वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक
हिसार : विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम) की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024 में भारत को 148 देशों में 131वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। यह न केवल दो पायदान की गिरावट है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में छुपी उस असमानता का पर्दाफाश भी करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब पूरी दुनिया लैंगिक असमानता को घटाने में धीमी किंतु स्थिर प्रगति कर रही है, तब भारत का पिछड़ना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि नीति, सोच और संस्थागत व्यवस्था की विफलता का प्रतिबिंब है।
वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक (ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स), जिसे 2006 में शुरू किया गया था, चार प्रमुख क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को मापता है—आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण। भारत का कुल स्कोर 64.1% है, जो वैश्विक औसत 68.5% से काफी कम है। यही नहीं, दक्षिण एशिया में भी भारत बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देशों से पीछे है।
आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में भारत ने मामूली सुधार किया है, लेकिन महिलाओं की श्रम भागीदारी दर अभी भी 45.9% पर अटकी हुई है। महिलाएँ मुख्यतः देखभाल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कम वेतन वाले क्षेत्रों में केंद्रित हैं। घरेलू और अवैतनिक श्रम, जो देश की असंगठित अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अभी तक किसी राष्ट्रीय लेखांकन में शामिल नहीं किया गया है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान कार्य के लिए 20–30% कम वेतन प्राप्त होता है। यह आर्थिक असमानता केवल आँकड़ों की नहीं, सोच की समस्या है।
शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति तो हुई है, परंतु महिला साक्षरता दर अभी भी लगभग 70% है, जो वैश्विक औसत 87% से बहुत कम है। उच्च शिक्षा, विशेषकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और निम्नवर्गीय परिवारों की लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने वाली सामाजिक बाधाएँ—जैसे बाल विवाह, रुढ़िवादी सोच और विद्यालयों की दूरी—अब भी मौजूद हैं।
स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के पैमाने पर भी भारत पिछड़ा हुआ है। जन्म के समय लिंग अनुपात अब भी 929 लड़कियाँ प्रति 1000 लड़कों के आसपास है। मातृत्व से जुड़ी समस्याएँ, कुपोषण, रक्ताल्पता (एनीमिया), और प्रसवकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। घर की चारदीवारी में महिलाओं की सेहत को प्राथमिकता न मिलना हमारी पारिवारिक व्यवस्था की कमजोरी है।
राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व घटकर 13.8% रह गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल 5.6% महिलाएँ हैं। यह तब और विडंबनापूर्ण हो जाता है जब हम जानते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित हो चुका है, परंतु जनगणना और निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण की प्रक्रिया के विलंब के कारण उसका क्रियान्वयन अटका हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल कानून पारित करना पर्याप्त नहीं, उन्हें लागू करने की इच्छाशक्ति भी आवश्यक है।
भारत को अपने पड़ोसी देशों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश जैसे देश ने सूक्ष्म वित्त, महिला शिक्षा प्रोत्साहन, और निरंतर राजनीतिक भागीदारी जैसे उपायों से सकारात्मक सुधार किए हैं। नेपाल में संविधान द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई निम्न आय वाले देशों ने धनी देशों की तुलना में लैंगिक समानता में अधिक तेजी से प्रगति की है, जो यह दर्शाता है कि बदलाव के लिए धन नहीं, दृढ़ नीयत चाहिए।
लैंगिक समानता केवल एक सामाजिक उद्देश्य नहीं, भारत की आर्थिक प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। मैकिंज़ी ग्लोबल संस्थान का अनुमान है कि यदि भारत कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाता है, तो 2025 तक अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 700 अरब डॉलर तक की वृद्धि कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन में महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक परिणाम भी अधिक न्यायसंगत और समावेशी होते हैं। भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता तभी सार्थक होगी, जब उसमें महिलाओं की पूरी और समान भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
किन्तु चुनौतियाँ गहरी हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्य, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमी, डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुँच और नीतियों के क्रियान्वयन में ढिलाई—ये सभी मिलकर लैंगिक असमानता को टिकाऊ बना रहे हैं।
अब समय आ गया है कि भारत केवल योजना बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें ज़मीन पर उतारे। महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने हेतु जनगणना और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। घरेलू और अवैतनिक श्रम को राष्ट्रीय आर्थिक लेखा-जोखा में शामिल कर उसे सम्मान और सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। महिलाओं के लिए लचीले और सुरक्षित कार्यस्थलों की व्यवस्था की जाए, विशेषकर ग्रामीण एवं अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में।
निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों में महिला निदेशक की अनिवार्यता हो। विज्ञान, राजनीति और उद्यमिता में महिलाओं के लिए परामर्श (मेंटॉरशिप) कार्यक्रम चलाए जाएँ। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए महिलाओं को सस्ते मोबाइल व इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को पंचायत स्तर तक पहुँचाया जाए।
हर योजना और सर्वेक्षण में लैंगिक रूप से अलग आँकड़े संकलित करना अनिवार्य हो ताकि राज्य और जिले स्तर पर प्रगति की निगरानी की जा सके और नीति निर्माण अधिक लक्षित हो सके।
भारत की लैंगिक समानता में यह गिरावट केवल एक आँकड़ा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है—कि हमने विकास की दौड़ में आधी आबादी को पीछे छोड़ दिया है। यह भूल केवल सामाजिक न्याय की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि की भी कीमत वसूलती है।
समानता की राह लंबी है, पर असंभव नहीं। नीति बन चुकी है, दिशा स्पष्ट है, अब आवश्यकता है राजनीतिक संकल्प, सामाजिक सहमति और संस्थागत क्रियान्वयन की। जब तक भारत अपनी आधी आबादी को बराबरी का स्थान नहीं देगा, तब तक “विकसित राष्ट्र” का सपना अधूरा रहेगा।
(प्रियंका सौरभ एक स्वतंत्र स्तंभकार, कवयित्री और सामाजिक विषयों पर मुखर लेखिका हैं। वे विशेष रूप से महिला अधिकार, शिक्षा और ग्रामीण भारत की आवाज़ को अपने लेखन में प्राथमिकता देती हैं।)
प्रियंका सौरभ।