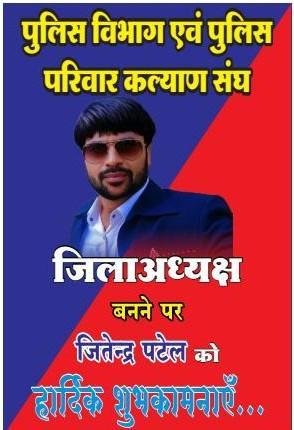एक राष्ट्र-एक चुनाव जनहित में क्रांतिकारी पहल

एक राष्ट्र-एक चुनाव जनहित में क्रांतिकारी पहल
लेखक : मदन मोहन छाबड़ा, प्रदेश सह संयोजक, एक राष्ट्र-एक चुनाव समिति
कुरुक्षेत्र,वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक : विश्व में भारत आर्थिक रूप से सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। लिहाजा, हर देशवासी का सपना है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मगर देश के विकास में चुनाव चक्र सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। इस चुनावी चक्र की बाधा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट-एक चुनाव की परिकल्पना की है, जोकि जनहित में क्रांतिकारी पहल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश के विकास की इस सबसे बड़ी बाधा को हटाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। पीएम मोदी ने पार्टी हितों को पीछे छोड़कर देश हित में एक राष्ट्र-एक चुनाव की मुहिम को आगे बढ़ाया है। भाजपा की नीति देश पहले, पार्टी बाद की रही है। मगर देश में कुछ विपक्षी दल संवैधानिक संस्थाओं पर तथ्यहीन आरोप लगाकर बदनाम करने की मुहिम चला रहे हैं। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता द्वारा लिए गए निर्णयों का स्वागत होना चाहिए। इन राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखना चाहिए। ये व्यवस्था बाबा साहेब आंबेडकर की बनाई हुई व्यवस्था है। इसका सम्मान होना चाहिए।
एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा भारत में नयी नहीं है। संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद, 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के तीन आम चुनावों के लिए भी जारी रही। कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर 1971 में नए चुनाव हुए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पांच वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया। जबकि, आपातकाल की घोषणा के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कुछ ही, केवल आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोकसभाएं अपना पांच वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकीं। जबकि छठी, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं सहित अन्य लोकसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में राज्य विधानसभाओं को भी इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है। विधानसभाओं को समय से पहले भंग किया जाना और कार्यकाल विस्तार बार-बार आने वाली चुनौतियां बन गए हैं। इन घटनाक्रमों ने एक साथ चुनाव के चक्र को अत्यंत बाधित किया, जिसके कारण देश भर में चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव का मौजूदा स्वरूप सामने आया है।
देश में बार-बार चुनाव होने से राष्ट्र के संसाधनों के साथ-साथ राष्ट्र के अमूल्य समय और धन की बर्बादी की होती है। युवा वर्ग देश हित में विकास की इस बड़ी बाधा को हटाने में सक्षम और समर्थ है। विशेषकर छात्र नेताओं को देश हित में अपनी अग्रणी और निर्णायक भूमिका निभानी होगी। बार-बार चुनावी प्रकिया से देश में विकास कार्य ठप्प हो जाते हैं। शासन प्रशासन नीतिगत निर्णय तक नहीं ले पाते जिससे विकास की नहीं रोजमर्रा के कामों की गति भी रुक जाती है। इस व्यवस्था से प्रशासनिक बोझ कम था, मतदाताओं को सुविधा थी और चुनाव आयोग पर भी दबाव नहीं पड़ता था। लेकिन यह संतुलन ज्यादा समय तक नहीं टिक सका।
अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं एक राष्ट्र-एक चुनाव के राष्ट्रीय संयोजक शिवराज चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में आगामी रणनीति तैयार की गई, जिसमें एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर विधानसभा स्तर पर जनमत अभियान शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय और कालेजों में जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। हरियाणा में यूथ को एक राष्ट्र-एक चुनाव के साथ जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों में संगोष्ठियों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है। यूथ को अवगत कराया जाएगा कि अलग-अलग समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। खासकर जो योजनाएं तैयार की गई जाती है, उनके क्रियान्वयन में भी बाधा आती है। अलग-अलग समय में चुनाव होने से सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़ा वर्ग और दलितों को होता, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने से उनके लिए तैयार की गई योजनाएं लागू नहीं हो पाती हैं।
शासन में निरंतरता को बढ़ावा : देश के विभिन्न भागों में चल रहे चुनावों के कारण, राजनीतिक दल, उनके नेता, विधायक तथा राज्य और केंद्र सरकारें अक्सर शासन को प्राथमिकता देने के बजाय आगामी चुनावों की तैयारी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक साथ चुनाव कराने से सरकार का ध्यान विकासात्मक गतिविधियों और जन कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा।
नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगी : चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन से नियमित प्रशासनिक गतिविधियां और विकास संबंधी पहल बाधित होती हैं। यह व्यवधान न केवल महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में बाधा डालता है, बल्कि शासन संबंधी अनिश्चितता को भी जन्म देता है। एक साथ चुनाव कराने से आचार संहिता के लंबे समय तक लागू होने की संभावना कम होगी, जिससे नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगी और शासन में निरंतरता संभव होगी।
संसाधनों को कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा : चुनाव ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की तैनाती, जैसे कि मतदान अधिकारी और सरकारी अधिकारियों को उनकी मूल जिम्मेदारियों से हटाकर चुनाव कार्यों में लगाना संसाधनों के उपयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक साथ चुनाव आयोजित होने से, बार-बार तैनाती की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे सरकारी अधिकारी और सरकारी संस्थाएं चुनाव-संबंधी कार्यों के बजाय अपनी प्राथमिक भूमिकाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता बनी रहेगी : एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम नहीं होती। वास्तव में, यह चुनावों के दौरान उनकी अधिक स्थानीयकृत और केंद्रित भूमिका को प्रोत्साहित करता है। इससे क्षेत्रीय दल अपनी अहम चिंताओं और आकांक्षाओं को उजागर कर पाते हैं। यह व्यवस्था एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनाती है जिसमें स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय चुनाव अभियानों से प्रभावित नहीं होते, इस प्रकार क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने वालों की प्रासंगिकता बनी रहती है।
राजनीतिक अवसरों में वृद्धि : एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों में अवसरों और जिम्मेदारियों का न्यायोचित तरीके से आवंटन होता है। वर्तमान में, किसी पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का चुनावी परिदृश्य पर हावी होना, कई स्तरों पर चुनाव लड़ना और प्रमुख पदों पर एकाधिकार असामान्य नहीं है। एक साथ चुनाव के परिदृश्य में, विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच विविधता और समावेशिता की अधिक गुंजाइश होती है, जिससे नेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला उभर कर सामने आती है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अहम योगदान देती है।
शासन पर ध्यान : देश भर में चल रहे चुनावों का चल रहा चक्र सुशासन से ध्यान भटकाता है। राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव-संबंधी गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे विकास और आवश्यक शासन के लिए कम समय बचता है। एक साथ चुनाव पार्टियों को मतदाताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित करने की अनुमति देते हैं, जिससे संघर्ष और आक्रामक प्रचार की घटनाओं में कमी आती है।
वित्तीय बोझ में कमी : एक साथ चुनाव कराने से कई चुनाव चक्रों से जुड़े वित्तीय खर्च में काफी कमी आ सकती है। यह मॉडल प्रत्येक व्यक्तिगत चुनाव के लिए मानव-शक्ति, उपकरणों और सुरक्षा संबंधी संसाधनों की तैनाती से संबंधित व्यय को घटाता है। इससे होने वाले आर्थिक लाभों में संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन शामिल हैं, जो आर्थिक विकास और निवेशकों के विश्वास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है।