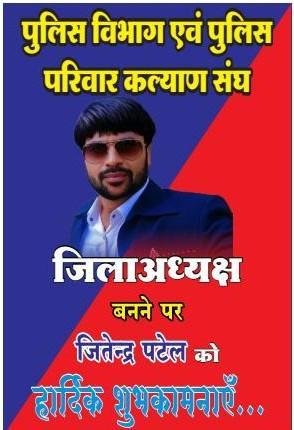सांस पर सिफारिश भारी: एक मासूम की मौत और सिस्टम की शर्मनाक चुप्पी : प्रियंका सौरभ

सांस पर सिफारिश भारी: एक मासूम की मौत और सिस्टम की शर्मनाक चुप्पी : प्रियंका सौरभ
वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक
हिसार : एक साल की मासूम बच्ची की जान इसलिए चली गई क्योंकि उसे 7 घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों ने सिफारिश लाने पर ही इलाज देने की बात कही। यह घटना पीजीआई रोहतक की व्यवस्था पर गहरा सवाल उठाती है। प्रश्न जो जलते रहेंगे। क्या सिफ़ारिश से ऊपर कभी जीवन होगा? क्या अस्पतालों में इलाज अब “पहचान-पत्र” बन गया है? क्या सरकारी संस्थानों में अब सिर्फ़ रसूख वाले ही सांस ले सकते हैं ?
01 जून 2025 को छपी रोहतक की एक खबर ने पूरे हरियाणा को हिला दिया। एक साल की मासूम बच्ची, जिसे सोनीपत से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था, सिर्फ़ इसलिए मौत के हवाले हो गई क्योंकि उसे सात घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला। परिवार का आरोप और भी ज्यादा डराने वाला है—डॉक्टरों ने कहा, सिफारिश लाओ, तभी मिलेगा इलाज।
यह घटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि उस सिस्टम की पोल खोलती है जो आम आदमी के जीवन को तंत्र की औपचारिकताओं में रौंद देता है। यह लेख सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं, हमारे पूरे स्वास्थ्य ढांचे की हत्या पर प्रश्नचिह्न है।
ज़िंदा रहने के लिए सिफारिश?
भारत के संविधान में स्वास्थ्य को एक मूल अधिकार माना गया है। लेकिन जब अस्पतालों के गलियारों में सिफारिश, जात, रसूख, और पहचान ही इलाज का मापदंड बन जाए, तो क्या यह संविधान भी केवल कागज़ी दस्तावेज़ रह जाता है?
मासूम बच्ची की मौत के मामले में भी, यह आरोप गंभीर है कि अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों ने इलाज को सिफारिश से जोड़ा। एक तरफ डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, दूसरी तरफ माँ की गोद में तड़पती बच्ची के लिए सात घंटे तक वेंटिलेटर न मिलना, इस “भगवान” की चुप्पी और संवेदनहीनता की हद दिखाता है।
व्यवस्था की निर्लज्जता।
पीजीआई रोहतक जैसे संस्थान, जो हरियाणा और आसपास के राज्यों के लिए “रेफरल सेंटर” की भूमिका निभाते हैं, वहाँ इस तरह की लापरवाही का मतलब है कि पूरे सिस्टम में सड़न आ चुकी है।
क्या वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था? नहीं।
क्या डॉक्टरों की टीम मौजूद नहीं थी? थी।
तो फिर समस्या क्या थी?
समस्या यह है कि हर सरकारी सुविधा अब भी एक “संबंधों की दौड़” बन गई है। इलाज पाने का हक़ आपके आर्थिक या सामाजिक दर्जे से तय होता है, न कि इंसान होने की बुनियादी पहचान से।
एक पिता की असहायता, एक माँ की चीख।
अखबार में छपी तस्वीरें सिर्फ दृश्य नहीं हैं, वो एक देश की आत्मा पर लगे दाग हैं। माँ अपनी मासूम बेटी की साँसों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और पिता इलाज के नाम पर दर-दर भटकता रहा। दोपहर 2 बजे जो बच्ची दाखिल हुई, उसकी मौत रात 9 बजे हो गई। सात घंटे, जिसमें केवल इंतज़ार लिखा गया था उसकी किस्मत में।
क्या ये वही देश है, जो “माँ” के नाम पर सरकारें चला लेता है? क्या ये वही प्रदेश है, जो “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का नारा देता है? क्या हमारी राजनीति अब सिर्फ़ भाषणों और विज्ञापनों तक सिमट गई है?
सवाल जो जनता को पूछने होंगे।
इस घटना से कुछ जरूरी और असहज सवाल पैदा होते हैं:
क्या सरकारी अस्पताल आम आदमी के लिए अब भी सुलभ हैं?
क्या इलाज सिफारिश या राजनीतिक जुड़ाव से मिलना चाहिए?
अगर पीड़ित बच्ची किसी मंत्री या अफ़सर की होती, तो क्या वेंटिलेटर मिल जाता?
क्या कोई ज़िम्मेदारी तय होगी? या हमेशा की तरह जांच कमेटी बना दी जाएगी?
नेताओं की चुप्पी और मीडिया की सीमाएँ
आज अगर कोई क्रिकेटर आउट हो जाए या कोई फिल्म रिलीज़ हो, तो न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग चलती है। लेकिन जब एक बच्ची तड़प-तड़प कर मर जाती है, तो यह सिर्फ़ एक लोकल कॉलम बनकर रह जाता है। बड़े नेताओं, मंत्रियों, और स्वास्थ्य विभाग के अफ़सरों की इस चुप्पी की भी जांच होनी चाहिए। क्या एक जान की कीमत इतनी कम हो चुकी है?
दोषी कौन: डॉक्टर, सिस्टम या हम सब?
डॉक्टरों पर उंगली उठाना आसान है। लेकिन असल दोषी तो वो सिस्टम है, जो एक सामान्य नागरिक को भीख माँगने की स्थिति में डाल देता है। दूसरी तरफ, हम सब भी दोषी हैं जो हर बार इन घटनाओं को पढ़कर अगले दिन भूल जाते हैं।
जब तक आम नागरिक सड़कों पर उतर कर सवाल नहीं पूछेगा, जब तक हम स्वास्थ्य को चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक ये व्यवस्थाएँ यूँ ही मासूमों की लाशों पर खामोशी से खड़ी रहेंगी।
अब क्या किया जाए? समाधान क्या है?
स्वास्थ्य क्षेत्र में जवाबदेही तय हो: पीजीआई जैसी संस्थाओं में यदि लापरवाही होती है तो उच्चस्तरीय जांच के बाद ज़िम्मेदार अफ़सर और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम: अस्पतालों में वेंटिलेटर, ICU और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का एक डिजिटल सार्वजनिक डैशबोर्ड होना चाहिए।
फ्री हेल्थ सर्विसेज़ की निगरानी: ग़रीबों के लिए घोषित स्वास्थ्य योजनाएँ ज़मीन पर कैसे लागू हो रही हैं, इसकी नियमित जांच और सामाजिक ऑडिट जरूरी हैं।
जन-जागरण और मीडिया की ज़िम्मेदारी: इस तरह की खबरों को दबाने या भूलने नहीं देना चाहिए। पत्रकारों, लेखकों, और नागरिक समाज को इसे निरंतर मुद्दा बनाए रखना होगा।
अंत में: एक बच्ची का मरना सिर्फ मौत नहीं, एक देश की हार है
उस मासूम ने कुछ नहीं माँगा था — न कोटा, न रिश्ता, न धर्म देखा, न जात। बस वो जीना चाहती थी। लेकिन हमारी व्यवस्था ने उसे सिखा दिया कि भारत में साँस लेने के लिए भी सिफारिश चाहिए।
इस लेख के अंत में, हम सबको खुद से यह पूछना चाहिए — > “अगर कल मेरी बेटी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, तो क्या मुझे भी सिफारिश लानी होगी?”
यदि इस सवाल ने आपको भीतर तक झकझोर दिया हो, तो इस लेख को साझा करें — ताकि वो बच्ची सिर्फ आंकड़ा न बने, बल्कि एक परिवर्तन की शुरुआत बन जाए।